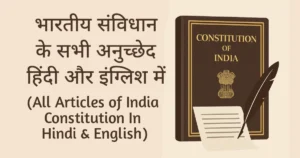जानें भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद हिंदी और इंग्लिश में सरल भाषा में। (Complete list of all Articles of Indian Constitution in Hindi & English for easy understanding.)
भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान माना जाता है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। अगर आप भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद (Articles) को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां हमने संविधान के हर अनुच्छेद को क्रमवार, सरल भाषा में हिंदी और उसके अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ पेश किया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए आपकी तैयारी और भी आसान हो सके।
भाग 1 – संघ और उसका राज्य क्षेत्र
Part 1 – The Union and its Territory
(अनुच्छेद 1 से 4 | Articles 1 to 4)
अनुच्छेद 1: भारत – राज्यों का संघ
Article 1: Name and territory of the Union
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 हमारे देश का नाम और उसकी संरचना बताता है। इसमें कहा गया है कि “भारत, अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा।” इसका अर्थ यह है कि भारत अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिलकर बना है, लेकिन यह एकजुट और अटूट देश है। भारत का क्षेत्र तीन हिस्सों से मिलकर बना है — राज्यों से, केंद्रशासित प्रदेशों से और उन क्षेत्रों से जिन्हें भविष्य में भारत में शामिल किया जा सकता है। संविधान ने भारत को संघ कहा है क्योंकि यहाँ राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर है और कोई भी राज्य भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार भारत राज्यों का समूह होते हुए भी एक अखंड राष्ट्र है।
Article 1 of the Indian Constitution defines the name and structure of our country. It states that “India, that is Bharat, shall be a Union of States.” This means that India is made up of different states and union territories, but it remains a united and indestructible nation. The territory of India consists of three parts — the states, the union territories, and any territories that may be acquired in the future. The Constitution uses the word Union to signify that the existence of states depends on the Centre, and no state has the right to secede from India. Thus, India, though a group of states, is an indivisible nation.
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश
Article 2: Admission or establishment of new States
अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भारत के बाहर के किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सके या भारत के भीतर एक नया राज्य स्थापित कर सके। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनना चाहता है या भारत उसे अपने में सम्मिलित करना चाहता है, तो संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत ने 1975 में सिक्किम को अपना 22वां राज्य बनाया। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे जनमत संग्रह के बाद भारत में मिलाया गया।
Article 2 empowers Parliament to admit into the Union of India any territory that is not already a part of India, or to establish a new state within India. This means if a foreign territory wishes to join India or India decides to incorporate it, Parliament can do so by enacting a law with a simple majority. For example, under Article 2, India admitted Sikkim as its 22nd state in 1975, which was earlier an independent kingdom and became part of India after a referendum.
अनुच्छेद 3: राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन
Article 3: Formation and alteration of States
अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का विभाजन कर सकती है, दो या अधिक राज्यों को मिला सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है या उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है। ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उस प्रस्ताव पर राय (सिफारिश) मांगते हैं, लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती। संसद साधारण बहुमत से यह कानून बना सकती है। इस अनुच्छेद के तहत कई बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, जैसे 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण और 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन।
Article 3 empowers Parliament to reorganize the states of India by enacting a law. Parliament can create a new state, merge two or more states, divide a state, alter the boundaries of a state, or even change the name of a state. Before doing so, the President seeks the opinion of the legislature of the concerned state, but this opinion is not binding on Parliament. Such changes can be made by Parliament through a simple majority. This Article has been used several times to reorganize states, such as the creation of Uttarakhand, Jharkhand, and Chhattisgarh in 2000, and the formation of Telangana in 2014 by bifurcating Andhra Pradesh.
अनुच्छेद 4: संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं
Article 4: No need of constitutional amendment
संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद द्वारा राज्यों के निर्माण, नाम बदलने या सीमाओं में बदलाव के लिए बनाए गए कानूनों के कारण संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं, उन्हें “संविधान संशोधन” नहीं माना जाता। ऐसे बदलावों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष संशोधन प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। संसद साधारण बहुमत से यह कर सकती है।
Under Article 4 of the Constitution, any changes made to the First and Fourth Schedules as a result of laws enacted under Articles 2 and 3 (regarding creation, renaming, or alteration of states) are not considered constitutional amendments. Such changes do not require the special procedure of Article 368 and can be carried out by Parliament through ordinary legislation.
भाग 2 – नागरिकता
Part 2 – Citizenship
(अनुच्छेद 5 से 11 | Articles 5 to 11)
अनुच्छेद 5: भारत की नागरिकता (26 जनवरी 1950 को)
Article 5: Citizenship at the commencement of the Constitution
अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के दिन भारतीय नागरिकता का प्रावधान करता है। यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे। इस दिन भारतीय नागरिक वही व्यक्ति होगा जो भारत में जन्मा हो, या जिसके माता या पिता भारत में जन्मे हों, या जिसने संविधान लागू होने से पहले कम-से-कम 5 साल तक भारत में निवास किया हो और उस दिन भारत में रह रहा हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का भारत के साथ गहरा संबंध था, उन्हें स्वतः भारतीय नागरिकता दे दी गई।
Article 5 provides for Indian citizenship at the commencement of the Constitution. It defines who shall be deemed an Indian citizen on 26 January 1950. Any person who was born in India, or whose parents were born in India, or who had been ordinarily residing in India for at least five years before the commencement and was present in India on that day, shall be considered an Indian citizen. This ensured that all those who had a strong connection with India automatically became its citizens on the day the Constitution came into force.
अनुच्छेद 6: पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता
Article 6: Citizenship of migrants from Pakistan
19 जुलाई 1948 से पहले भारत लौटने वाले पाकिस्तान से आए लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे।
19 जुलाई 1948 के बाद लौटने वालों को नागरिकता के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकरण कराना होगा।
Persons who migrated from Pakistan to India before 19 July 1948 are deemed Indian citizens.
Those who came after 19 July 1948 must register with the prescribed authority to obtain citizenship.
अनुच्छेद 7: पाकिस्तान चले गए लोग
Article 7: Rights of certain migrants to Pakistan
अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में है जो भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए थे। ऐसे लोग जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाकर वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, वे भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया और बाद में भारत लौट आया और सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वापस आकर भारत में बस गया, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह था कि जो लोग स्थायी रूप से पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर चुके थे, उन्हें भारतीय नागरिक न माना जाए, लेकिन जिनका इरादा भारत लौटने का था, उन्हें मौका दिया जाए।
Article 7 deals with people who migrated to Pakistan during the Partition of India. Any person who migrated to Pakistan after 1 March 1947 and acquired Pakistani citizenship is not considered an Indian citizen. However, if a person migrated to Pakistan but later returned to India and resettled here in accordance with the laws made by the Government of India, they could be granted Indian citizenship. The purpose of this article was to deny Indian citizenship to those who had permanently chosen Pakistan but allow those who intended to return to India an opportunity to reclaim their citizenship.
अनुच्छेद 8: विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग
Article 8: Citizenship of Indians living abroad
अनुच्छेद 8 उन लोगों के अधिकारों से जुड़ा है जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर रह रहे थे लेकिन भारतीय मूल के थे। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ था, या जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में जन्मे थे और जो किसी दूसरे देश में रह रहे थे, उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार दिया गया। इसके लिए शर्त यह थी कि वे उस देश में भारतीय मिशन या भारत सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिक प्रतिनिधि के पास जाकर खुद को पंजीकृत कराएं। इस प्रावधान का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपने देश से जोड़कर रखना था।
Article 8 relates to the rights of persons of Indian origin who were living outside India at the commencement of the Constitution. Any person who was born in India, or whose parents or grandparents were born in India, and who was residing in another country, was entitled to Indian citizenship. The condition was that they had to register themselves as Indian citizens with the diplomatic or consular representative of India in that country. The purpose of this provision was to maintain the connection of persons of Indian origin living abroad with their homeland.
अनुच्छेद 9: दोहरी नागरिकता पर रोक
Article 9: No dual citizenship
अनुच्छेद 9 भारतीय नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है। यदि कोई व्यक्ति, जो भारतीय नागरिक है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता के साथ-साथ किसी अन्य देश की नागरिकता रखना संविधान के अनुसार संभव नहीं है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया ताकि नागरिकों की निष्ठा केवल भारत के प्रति बनी रहे।
Article 9 prohibits dual citizenship for Indian citizens. If a person, who is an Indian citizen, voluntarily acquires the citizenship of another country, they cease to be an Indian citizen. This means that one cannot hold Indian citizenship along with the citizenship of another country at the same time. This provision ensures that the allegiance of citizens remains solely to India.
अनुच्छेद 10: नागरिकता का अधिकार जारी रहेगा
Article 10: Continuance of rights of citizenship
अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद इसके विपरीत कोई कानून नहीं बना देती। इसका अर्थ है कि संविधान लागू होने के समय जो लोग भारतीय नागरिक थे, वे भारतीय नागरिक बने रहेंगे और उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जब तक कि संसद द्वारा कोई नया प्रावधान न किया जाए। यह नागरिकों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है।
Article 10 ensures that the citizenship of Indian citizens shall continue unless and until Parliament makes a law to the contrary. This means that a person who is a citizen at the commencement of the Constitution shall remain a citizen, and their citizenship cannot be taken away arbitrarily unless provided by a law enacted by Parliament. This gives stability and protection to citizens.
अनुच्छेद 11: संसद को कानून बनाने का अधिकार
Article 11: Parliament’s power to regulate citizenship
अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वह भारतीय नागरिकता से जुड़े विषयों पर कानून बना सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता से संबंधित सभी मामलों — जैसे नागरिकता प्राप्त करने, उसे खोने या बनाए रखने के नियम — संसद द्वारा तय किए जाएंगे। इसलिए भारत में नागरिकता से जुड़े सभी प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए हैं।
Article 11 empowers Parliament to make laws relating to citizenship. It makes it clear that all matters regarding citizenship — such as acquisition, termination, or continuation of citizenship — shall be governed by laws made by Parliament. Accordingly, all the rules regarding citizenship in India are provided under the Citizenship Act, 1955.
भाग 3 – मौलिक अधिकार
Part 3 – Fundamental Rights
(अनुच्छेद 12 से 35 | Articles 12 to 35)
भारतीय संविधान का भाग 3 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव (रीढ़) हैं और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ जीने का हक़ देते हैं। मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक के इन अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। संविधान में इन अधिकारों को 6 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है।
Part 3 of the Indian Constitution guarantees Fundamental Rights to the citizens. These rights are the backbone of Indian democracy and ensure that every individual can live with freedom, equality, and justice. They protect citizens against any arbitrary action by the state or others. The Constitution classifies these rights into 6 main types.
- समानता का अधिकार (Right to Equality)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
- समानता का अधिकार (Right to Equality)
समानता का अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को कानून के सामने समानता और किसी भी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा देता है। इस अधिकार के तहत हर नागरिक जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव के बिना समान दर्जा पाने का हक़दार है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न प्रावधान हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 किसी सार्वजनिक स्थान या सेवा में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 18 नागरिकों को उपाधियों (Titles) से मुक्त रखता है ताकि कोई सामाजिक असमानता न हो। यह अधिकार देश में बराबरी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की नींव है।
Right to Equality:
The Right to Equality is one of the most important Fundamental Rights in the Indian Constitution. It guarantees equality before the law and protection from any kind of discrimination. Every citizen has the right to equal status without discrimination on the grounds of religion, caste, gender, place of birth, or race. This right is covered under Articles 14 to 18. Article 14 ensures equality before the law. Article 15 prohibits discrimination in access to public places or services. Article 16 guarantees equal opportunity in public employment. Article 17 abolishes untouchability and declares it a punishable offence. Article 18 prohibits the state from conferring titles to prevent social inequality. This right forms the foundation of equality and social justice in India. - स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक प्रमुख मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक फैला हुआ है और कई प्रकार की स्वतंत्रताओं को शामिल करता है। अनुच्छेद 19 हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, किसी भी राज्य में बसने का अधिकार और अपनी पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 20 अपराध के मामलों में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिकार हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भर और सम्मानित बनने का अवसर देता है।
Right to Freedom:
The Right to Freedom is a key Fundamental Right in the Indian Constitution, which guarantees citizens personal liberty and a dignified life. This right is covered under Articles 19 to 22 and includes several types of freedoms. Article 19 grants every citizen the freedom of speech and expression, the right to assemble peacefully, to form associations or unions, to move freely throughout the country, to reside in any part of India, and to practice any profession or trade of their choice. Article 20 provides protection to citizens in criminal cases, and Article 21 guarantees the right to life and personal liberty in accordance with the procedure established by law. Article 22 ensures certain rights for arrested persons. This right allows individuals to live independently and with dignity. - शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)
शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो नागरिकों को हर तरह के शोषण से सुरक्षा देता है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी मर्ज़ी के खिलाफ काम नहीं करवाया जा सकता और न ही किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत मानव तस्करी (Trafficking) और बच्चों को खतरनाक कामों में लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाई गई है। इस अधिकार का उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।
Right Against Exploitation:
The Right Against Exploitation is an important Fundamental Right in the Indian Constitution that protects citizens from all forms of exploitation. This right ensures that no person can be forced to work against their will or be subjected to bonded labour. It completely prohibits human trafficking and employing children in hazardous occupations. For example, Article 23 of the Constitution prohibits human trafficking, bonded labour, and forced labour. Article 24 prohibits employing children below the age of 14 in factories, mines, or other hazardous work. The purpose of this right is to protect the weaker sections of society and to ensure them a life of dignity. - धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को यह अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों को संचालित करने और धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर लगाने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करता है। यह अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने में मदद करता है और हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
Right to Freedom of Religion:
The Right to Freedom of Religion guarantees that Indian citizens can freely profess, practice, and propagate the religion of their choice. This right is provided under Articles 25 to 28 of the Constitution. Article 25 allows every individual the freedom to follow, practice, and spread their religion. Article 26 grants religious communities the right to manage their own religious affairs and property. Article 27 prohibits the state from imposing taxes to promote any particular religion. Article 28 clarifies provisions regarding religious education. This right helps maintain India’s secular character and ensures that every citizen enjoys religious freedom. - संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी भाषा, संस्कृति और शिक्षा की रक्षा के लिए दिया गया है। यह अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकें। इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में रहने वाले विभिन्न धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अपनी पहचान बनाए रखें और उन्हें बराबरी के साथ विकास करने का अवसर मिले।
Cultural and Educational Rights:
The Cultural and Educational Rights are provided in the Indian Constitution to protect the language, culture, and education of minority communities. These rights are enshrined in Articles 29 and 30. Article 29 gives citizens belonging to any section of society the right to preserve their distinct language, script, and culture. Article 30 grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. The aim of this right is to ensure that religious and linguistic minorities in India can maintain their unique identity and have equal opportunities for development. - संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को यह शक्ति देता है कि यदि उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वे सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय मांग सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसे भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इस अधिकार के तहत नागरिक कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट द्वारा हाबियस कॉर्पस, मंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी जैसी रिट्स जारी की जा सकती हैं। इस अधिकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार केवल दिखावे के न रह जाएं बल्कि उनका पालन वास्तव में हो।
Right to Constitutional Remedies:
The Right to Constitutional Remedies empowers Indian citizens to approach the High Court or the Supreme Court directly if any of their Fundamental Rights are violated. This right is provided under Article 32, which Dr. B. R. Ambedkar described as the heart and soul of the Constitution. Under this right, citizens can file petitions in the courts, and the courts can issue writs such as Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto, and Certiorari to enforce their rights. The purpose of this right is to ensure that Fundamental Rights are not just written guarantees but are actually enforced in practice.
अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा
Article 12: Definition of State
अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान में “राज्य” शब्द की परिभाषा देता है। इसके अनुसार राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधानसभाएं, स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम और पंचायतें) और वे सभी प्राधिकरण शामिल होते हैं जो सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। इसका महत्व यह है कि यदि इन संस्थाओं द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को अदालत में जाकर न्याय मांगने का अधिकार है। इस तरह अनुच्छेद 12 यह तय करता है कि किन-किन संस्थाओं पर मौलिक अधिकार लागू होते हैं।
Article 12 of the Indian Constitution defines the term “State”. According to this, the State includes the Central Government, State Governments, Parliament, State Legislatures, local authorities (like municipalities and panchayats), and all authorities under government control. The significance of this definition is that if any of these bodies violate a citizen’s Fundamental Rights, the citizen has the right to challenge such actions in a court of law. Thus, Article 12 clarifies which bodies are bound to respect Fundamental Rights.
अनुच्छेद 13: विधियों की असंवैधानिकता
Laws inconsistent with Fundamental Rights
अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। इसके अनुसार संविधान लागू होने के बाद संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वह उस हद तक अमान्य (null and void) माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसे रद्द कराया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है।
Article 13 is an important provision of the Indian Constitution that ensures no law can violate the Fundamental Rights of citizens. According to this article, any law made by Parliament or State Legislatures after the commencement of the Constitution, if found inconsistent with Fundamental Rights, shall be considered null and void to the extent of the violation. This means that citizens can challenge any such law in court, and the court has the power to strike it down. Article 13 acts as a safeguard to protect citizens’ rights.
1. समानता का अधिकार | Right to Equality (Art. 14–18)
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
Article 14: Equality before law and equal protection of laws
अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो हर नागरिक को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी ऊँची हैसियत या शक्ति रखता हो, कानून से ऊपर नहीं है। सभी नागरिकों के साथ समान परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसमें दो मुख्य सिद्धांत निहित हैं — पहला, कानून के समक्ष समानता, जिसका मतलब है कि सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं और किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक जैसा लागू होगा। इसका उद्देश्य पक्षपात को खत्म करना और समाज में न्याय व समानता सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अमीर या गरीब व्यक्ति अपराध करता है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। हालांकि, यह सिद्धांत सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाए, ताकि वास्तव में समानता स्थापित की जा सके। इस तरह अनुच्छेद 14 सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की आत्मा है।
Article 14 is one of the most important Fundamental Rights in the Indian Constitution, which guarantees every citizen equality before the law. This means that no person, regardless of their position or power, is above the law. All citizens will be treated equally under similar circumstances. It embodies two principles — first, equality before law, which ensures that everyone is equal in the eyes of the law and no special privileges are granted to anyone; and second, equal protection of laws, which means that under the same conditions, the law will apply equally to all individuals. The purpose of Article 14 is to eliminate discrimination and ensure justice and equality in society. For example, if a rich or poor person commits a crime, both will be treated equally by the law. However, this Article also allows the State to make special provisions for socially and economically disadvantaged groups in order to achieve real equality. Thus, Article 14 is the soul of social justice and democracy.
अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, आदि के आधार पर भेदभाव वर्जित
Article 15: Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, etc.
अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह अधिकार सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, पार्क, कुएं, होटल आदि के उपयोग और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में सभी को समान अवसर देता है। अनुच्छेद 15 का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और पिछड़े हुए वर्गों के प्रति centuries-old भेदभाव को खत्म करना है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बना सके। इसका मतलब है कि आरक्षण और विशेष योजनाएं इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं बल्कि इसका हिस्सा हैं ताकि वास्तविक समानता सुनिश्चित की जा सके।
Article 15 is an important provision of the Indian Constitution that ensures the State shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. This guarantees equal access to public places such as schools, parks, wells, hotels, and other facilities provided by the State. The purpose of Article 15 is to promote social equality and eliminate centuries-old discrimination against marginalized communities. This Article also empowers the State to make special provisions for socially and educationally backward classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and women. This means that reservations and special schemes are not a violation but an essential part of this Article to achieve substantive equality.
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
Article16: Equality of opportunity in public employment
अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों (सार्वजनिक रोजगार) में समान अवसर की गारंटी देता है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और सभी को योग्यता के आधार पर बराबरी से नौकरी पाने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाओं में भर्ती और पदोन्नति में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
हालांकि, इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यह विशेष प्रावधान इसलिए किए जाते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके और वास्तविक समानता कायम हो।
Article 16 is an important provision of the Indian Constitution that guarantees all citizens equal opportunity in matters of public employment (government jobs). It means the State shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any other factor, and everyone shall have an equal right to compete for government jobs based on merit. The purpose of this Article is to ensure fairness and transparency in recruitment and promotions in public services.
However, this Article also allows the government to make provisions for the reservation of posts in favor of socially and educationally backward classes, Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), and other disadvantaged groups. Such special provisions are intended to ensure equal opportunity and establish real equality in society.
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
Article 17: Abolition of Untouchability
अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का एक ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अस्पृश्यता की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप को कानूनन अपराध घोषित करता है। इसका अर्थ यह है कि अब किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या जन्म के आधार पर अछूत मानकर सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों, जलस्रोतों, स्कूलों या अन्य सुविधाओं के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का पालन करना या किसी को अस्पृश्य मानकर उसके साथ भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। इस प्रावधान ने भारतीय समाज में बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और सामाजिक न्याय की नींव रखी। इसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने ‘अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955’ भी पारित किया, जिसे अब सिविल राइट्स एक्ट कहा जाता है।
Article 17 is a historic and socially significant provision of the Indian Constitution. It completely abolishes the practice of untouchability and declares its practice in any form as a punishable offence. This means no person can be treated as an untouchable on the basis of caste or birth and cannot be denied access to public places, temples, water sources, schools, or other facilities. Practicing untouchability or discriminating against someone as an untouchable is a criminal offence under this Article. This provision marked a major step towards equality in Indian society and laid the foundation for social justice. To implement it, Parliament enacted the Untouchability (Offences) Act, 1955, which is now known as the Protection of Civil Rights Act.
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
Article18: Abolition of Titles
अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान में समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक अहम प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में विशेषाधिकार, भेदभाव और ऊँच-नीच को खत्म करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को ‘सर’, ‘रायबहादुर’, ‘नवाब’, जैसी उपाधियाँ दी जाती थीं, जिनसे कुछ व्यक्तियों को दूसरों से ऊँचा दिखाया जाता था। संविधान निर्माताओं ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया ताकि सभी नागरिक समान माने जाएं। इसलिए यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, न ही कोई विदेशी नागरिक भारत सरकार से उपाधि ले सकता है। यह प्रतिबंध केवल ऐसी उपाधियों पर लागू होता है, जो सम्मान और विशेषाधिकार देने के लिए होती हैं। हालांकि, शैक्षिक और सैन्य डिग्रियाँ, जैसे ‘डॉक्टर’, ‘प्रोफेसर’, ‘जनरल’ आदि, इस प्रतिबंध से बाहर हैं, क्योंकि ये योग्यता और कड़ी मेहनत का प्रतीक होती हैं। यह अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो हर नागरिक को समान सम्मान और अवसर सुनिश्चित करता है और समाज में ऊँच-नीच की मानसिकता को खत्म करता है।
Article 18 is a crucial provision of the Indian Constitution that preserves equality and democratic values by abolishing titles. Its primary aim is to eliminate privileges, discrimination, and a sense of superiority in society. During British rule, titles like ‘Sir’, ‘Rai Bahadur’, ‘Nawab’, etc., were conferred to create a hierarchy and elevate certain individuals above others. The Constitution makers abolished this practice to ensure that all citizens are seen as equals. Therefore, Article 18 states that no citizen of India shall accept any title from the State, and even a foreign citizen cannot accept a title from the Indian government. This prohibition applies only to honorific and hereditary titles that confer social prestige and privilege. However, academic and military distinctions like ‘Doctor’, ‘Professor’, ‘General’, etc., are exempt because they signify merit and hard work. This Article embodies the spirit of Indian democracy by ensuring equal respect and opportunity for all citizens and dismantling hierarchical thinking.
2. स्वतंत्रता का अधिकार | Right to Freedom (Art. 19–22)
अनुच्छेद 19: 6 स्वतंत्रताएं
Article 19: Protection of 6 Freedoms
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को 6 मौलिक स्वतंत्रताएँ देता है। ये स्वतंत्रताएँ लोकतंत्र की नींव हैं और हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर देती हैं। ये 6 स्वतंत्रताएँ इस प्रकार हैं:
Article 19 of the Indian Constitution guarantees 6 fundamental freedoms to every citizen. These freedoms form the foundation of democracy and allow individuals to express themselves and live with dignity. The 6 freedoms are as follows:
- वाणी की स्वतंत्रता (Freedom of speech)
- सभा की स्वतंत्रता (Right to assemble)
- संगठन बनाने की स्वतंत्रता (Form associations)
- देश में कहीं भी जाने का अधिकार (Move freely)
- भारत में कहीं भी रहने का अधिकार (Reside anywhere)
- कोई भी व्यवसाय/धंधा करने का अधिकार (Practice any profession)
1. वाणी की स्वतंत्रता (Freedom of Speech)
वाणी की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों को दी गई सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में से एक है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने, बोलने, लिखने, छापने और प्रचारित करने का अधिकार है। यह लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि बिना विचार व्यक्त किए लोकतांत्रिक बहस और निर्णय संभव नहीं। नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी राय प्रकट कर सकते हैं।
लेकिन यह स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, इस पर कुछ “यथोचित प्रतिबंध” लगाए जा सकते हैं, ताकि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और अदालत की अवमानना से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं दे सकता या झूठी अफवाहें फैलाकर हिंसा नहीं भड़का सकता।
इसलिए वाणी की स्वतंत्रता नागरिकों को अधिकार तो देती है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी देती है कि वे अपने शब्दों का प्रयोग समाज के हित में करें।
Freedom of Speech
Freedom of Speech is one of the most important freedoms guaranteed to citizens under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. It means that every citizen has the right to express their opinions through speech, writing, publishing, and dissemination of ideas. This is the soul of democracy, as democratic debate and informed decision-making are impossible without free expression. Citizens can criticize government policies, stage protests, and voice their opinions freely.
However, this freedom is not absolute. According to Article 19(2), reasonable restrictions can be imposed in the interests of the sovereignty and security of the country, public order, decency, morality, and to prevent contempt of court. For example, a person cannot deliver hate speeches or spread false rumors to incite violence.
Thus, Freedom of Speech gives citizens a right, but also imposes a duty to use their words responsibly for the greater good of society.
2. सभा की स्वतंत्रता (Right to Assemble)
सभा की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत दी गई एक मौलिक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने का अधिकार है। यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इससे नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का समर्थन या विरोध कर सकते हैं और सामाजिक मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठा सकते हैं। यह स्वतंत्रता नागरिकों को अपनी असहमति व्यक्त करने का अवसर देती है और लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ावा देती है।
हालांकि, यह स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं है। राज्य इस पर “यथोचित प्रतिबंध” लगा सकता है ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा और शांति बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर कोई सभा हिंसक हो जाती है या कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, तो प्रशासन उस पर रोक लगा सकता है। लेकिन शांतिपूर्ण और वैध सभा करना हर नागरिक का अधिकार है और इसे लोकतंत्र की ताकत माना जाता है।
Right to Assemble
The Right to Assemble is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(b) of the Indian Constitution. It means that every citizen has the right to assemble peacefully and without arms in public. This is an essential feature of democracy, as it allows citizens to express their opinions, support or oppose government policies, and raise their collective voice on social issues. This freedom gives people the opportunity to express dissent and promotes active participation in democratic processes.
However, this freedom is not absolute. The State can impose “reasonable restrictions” to maintain public order, security, and peace. For example, if an assembly turns violent or threatens law and order, the authorities can prohibit it. But the right to hold a peaceful and lawful assembly is a fundamental right of every citizen and is considered the strength of a democracy.
3. संगठन बनाने की स्वतंत्रता (Right to Form Associations)
संगठन बनाने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत नागरिकों को दी गई एक महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रता है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को संगठन, यूनियन, सहकारी समिति, क्लब, राजनीतिक दल या अन्य समूह बनाने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह लोगों को अपने साझा हितों के लिए संगठित होने और सामूहिक रूप से काम करने का अवसर देती है। उदाहरण के लिए, मज़दूर यूनियन बनाना, छात्र संगठन बनाना, या पेशेवर संगठनों में शामिल होना इस अधिकार के अंतर्गत आता है।
हालांकि, यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह असीमित नहीं है। राज्य इस पर “यथोचित प्रतिबंध” लगा सकता है, अगर कोई संगठन देश की संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के लिए खतरा पैदा करता है। उदाहरण के लिए, आतंकवादी संगठन, अपराधी गिरोह या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
इस प्रकार यह स्वतंत्रता नागरिकों को सामूहिक शक्ति का अनुभव कराती है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी देती है कि संगठन समाज और राष्ट्र के हित में हों।
Right to Form Associations
The Right to Form Associations is an important fundamental right guaranteed to citizens under Article 19(1)(c) of the Indian Constitution. It means that every person has the freedom to form associations, unions, cooperative societies, clubs, political parties, or other groups. This freedom is a vital part of democracy, as it allows people to organize themselves for common interests and work collectively. For example, forming trade unions, student organizations, or professional bodies comes under this right.
However, this freedom is also not unlimited. The State can impose “reasonable restrictions” if an association poses a threat to the sovereignty of the country, public order, or morality. For instance, terrorist groups, criminal gangs, or anti-national organizations can be banned.
Thus, this right empowers citizens to act collectively and strengthens democracy, but also comes with the responsibility to use it in the interest of society and the nation.
4. देश में कहीं भी जाने का अधिकार (Move Freely)
देश में कहीं भी जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने-जाने और घूमने-फिरने का अधिकार है। यह अधिकार नागरिकों को अपनी पसंद के राज्य, शहर या गाँव में यात्रा करने और वहाँ रहने की आज़ादी देता है। यह स्वतंत्रता भारत की एकता और अखंडता को मज़बूत करती है, क्योंकि सभी नागरिकों को पूरे देश में बराबरी का अधिकार मिलता है।
हालांकि, यह अधिकार भी पूरी तरह असीमित नहीं है। राज्य कुछ परिस्थितियों में इस पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे — जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करना ताकि वहाँ की संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली सुरक्षित रह सके, या किसी महामारी, कानून-व्यवस्था की समस्या, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। उदाहरण के लिए, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ‘इनर लाइन परमिट’ की आवश्यकता होती है।
इस प्रकार यह अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और देश के हर कोने तक पहुँचने का मौका देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
Right to Move Freely
The Right to Move Freely is an important fundamental right guaranteed under Article 19(1)(d) of the Indian Constitution. It means that every Indian citizen has the freedom to travel and move around freely throughout the territory of India. This right allows citizens to visit, travel, and explore any state, city, or village of their choice. It strengthens the unity and integrity of India by ensuring equal access to all parts of the country for every citizen.
However, this right is also not absolute. The State may impose reasonable restrictions in certain situations — such as to protect the culture and traditions of tribal areas by restricting outsiders, to maintain public order during an emergency, or for national security reasons. For example, in some northeastern states, an Inner Line Permit is required to enter.
Thus, this right gives citizens the freedom and opportunity to move anywhere in the country, while respecting certain necessary conditions.
5. भारत में कहीं भी रहने का अधिकार (Right to Reside Anywhere)
भारत में कहीं भी रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि हर भारतीय नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सके और निवास कर सके। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को देशभर में समानता का अनुभव कराता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी जन्मभूमि तक सीमित न रहे। इससे रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन की बेहतर परिस्थितियों के लिए लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं।
हालांकि, यह अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य कुछ परिस्थितियों में इस पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि — जनजातीय क्षेत्रों और विशेष संरक्षित क्षेत्रों में बाहरी लोगों के बसने पर रोक ताकि वहाँ की संस्कृति, जनजातीय अधिकार और पर्यावरण सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य कारणों से भी कुछ क्षेत्रों में बसने पर नियंत्रण किया जा सकता है।
इस प्रकार यह अधिकार नागरिकों को देशभर में स्वतंत्र रूप से रहने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही समाज और देश के हित में कुछ सीमाओं के अधीन रहता है।
Right to Reside Anywhere in India
The Right to Reside Anywhere in India is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(e) of the Constitution. It means that every Indian citizen has the freedom to settle and live in any part of the country. This right allows citizens to experience equality across India and ensures that no one is confined to their birthplace alone. It enables people to move from one state to another in search of better opportunities for employment, education, business, or an improved quality of life.
However, this right is also not unlimited. The State may impose reasonable restrictions under certain conditions. For example — restrictions on outsiders settling in tribal or protected areas to preserve their culture, rights, and environment. Similarly, in the interest of national security, public order, or public health, some areas may have controlled settlement.
Thus, this right empowers citizens to live anywhere in India freely, subject to certain necessary conditions for the greater good of society and the nation.
6. कोई भी व्यवसाय/धंधा करने का अधिकार (Right to Practice Any Profession)
कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा चुनने और करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय या उद्योग चुन सके और चला सके। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, उद्योग स्थापित करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तो उसे इस अधिकार के तहत अनुमति है।
हालांकि, यह अधिकार भी पूरी तरह असीमित नहीं है। राज्य इस पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है ताकि जनता के स्वास्थ्य, नैतिकता और कानून-व्यवस्था की रक्षा की जा सके। जैसे कि आप अवैध धंधा (जैसे मादक पदार्थों का व्यापार), खतरनाक उद्योग, या समाज के लिए हानिकारक कोई पेशा नहीं कर सकते। साथ ही, कुछ पेशों (जैसे डॉक्टर, वकील) के लिए सरकार ने योग्यता और लाइसेंस की शर्तें तय की हैं।
इस प्रकार यह अधिकार नागरिकों को आज़ादी देता है कि वे अपने कौशल और रुचि के अनुसार जीविका चला सकें, लेकिन यह भी सुनिश्चित करता है कि यह कार्य समाज और देश के हित के खिलाफ न हो।
Right to Practice Any Profession
The Right to Practice Any Profession, Trade, Business, or Occupation is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(g) of the Indian Constitution. It means that every citizen has the freedom to choose and carry on any profession, trade, business, or industry of their choice and ability. This right ensures equal opportunity and economic freedom in a democracy. For example, a person can choose to become a doctor, open a shop, set up an industry, or engage in trade under this right.
However, this right is not unlimited. The State can impose reasonable restrictions to protect public health, morality, and law and order. For instance, one cannot engage in illegal businesses (like drug trafficking), dangerous industries, or professions harmful to society. Also, for certain professions (like doctor, lawyer), the government prescribes qualifications and licenses.
Thus, this right gives citizens the freedom to earn a livelihood based on their skills and interests, while ensuring that their work does not harm the interests of society or the nation.
अनुच्छेद 20: अपराध के मामलों में सुरक्षा
Article 20: Protection in respect of conviction for offences
अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को अपराध के आरोप में गिरफ्तार या सज़ा दिए जाने पर कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और कानून का दुरुपयोग न किया जाए। यह अनुच्छेद तीन मुख्य प्रकार की सुरक्षा देता है:
पहली, पूर्वव्यापी दंड का निषेध (Ex Post Facto Law) — किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता जो अपराध उस समय न रहा हो, जब उसने उसे किया था। यानी पुराने कानूनों को पीछे जाकर लागू नहीं किया जा सकता।
दूसरी, दो बार सज़ा न होना (Double Jeopardy) — किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही सज़ा दी जाएगी।
तीसरी, आत्म-दोषारोपण के लिए मजबूर न करना (Self-incrimination) — किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
ये तीनों सुरक्षा हमारे कानूनी तंत्र में निष्पक्षता और नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं।
Article 20 is a significant fundamental right in the Indian Constitution that provides key legal protections to a person accused or convicted of an offence. Its purpose is to ensure that no injustice is done to any individual and the law is not misused. It provides three main protections:
First, Prohibition of Ex Post Facto Law — A person cannot be punished for an act that was not a crime when it was committed. In other words, laws cannot be applied retrospectively to punish someone.
Second, Protection against Double Jeopardy — No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.
Third, Protection against Self-incrimination — No person shall be compelled to testify against himself.
These three safeguards ensure fairness, justice, and protection of individual liberty in our legal system.
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
Article 21: Protection of life and personal liberty
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है, जो हमारे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह अधिकार हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करता है कि उसका जीवन और आज़ादी बिना किसी उचित कानून और कानूनी प्रक्रिया के छीनी नहीं जा सकती। इसमें केवल जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमा के साथ अच्छा और सुरक्षित जीवन जीने का हक़ भी शामिल है। जीवन का मतलब केवल शारीरिक रूप से जीवित रहना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना जिसमें इंसान को सम्मान, अच्छा वातावरण, स्वस्थ रहने का अवसर, शिक्षा और आजीविका भी मिले। इस अधिकार का लाभ भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को मिलता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो, विदेशी हो या कोई शरणार्थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह कहा है कि अनुच्छेद 21 में स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, यातनाओं से मुक्त रहने का अधिकार, कानूनी सहायता पाने का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है। यह अनुच्छेद यह भी तय करता है कि किसी को भी कानून के बिना जेल में बंद नहीं किया जा सकता, या उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। इसके तहत हर व्यक्ति को न्याय और कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार मिलता है। इस तरह अनुच्छेद 21 हर इंसान को न सिर्फ़ जीवित रहने बल्कि एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है।
Article 21 is considered the most important fundamental right in the Indian Constitution, as it protects our life and personal liberty. This article ensures that no person can be deprived of their life or freedom without proper law and legal procedure. The right to life does not just mean the right to exist physically, but also the right to live a good, safe, and dignified life. It includes the right to live with respect, in a clean and healthy environment, with access to health care, education, livelihood, and freedom from torture. This right is given to every person living in India — whether an Indian citizen, a foreign national, or even a refugee. The Supreme Court has said in many judgments that Article 21 also includes the right to clean air and water, the right to legal aid, the right to privacy, the right to social security, and the right to be free from illegal detention. No one can be put in jail or have their freedom taken away without following due process of law. In this way, Article 21 guarantees not just the right to live, but also the right to live a meaningful and dignified life for every person in India.
अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार
Article 21: Right to Education
अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। यह हमारे देश के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर बच्चे को स्कूल जाने का अवसर दे और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाए। इसमें न केवल स्कूल में दाखिला बल्कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा भी सुनिश्चित करना शामिल है। इसके लिए सरकार ने ‘मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ (Right to Education Act, 2009) बनाया, जिसे हम RTE Act कहते हैं। इस अधिनियम के तहत यह तय हुआ कि निजी स्कूलों को भी गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। शिक्षा का अधिकार केवल पढ़ने-लिखने का हक़ ही नहीं है, बल्कि यह बच्चों को सम्मान के साथ स्कूल में पढ़ाई का माहौल देने और उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनाने का भी माध्यम है। अनुच्छेद 21A यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी या किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित न रहे। इस तरह यह अधिकार हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है और देश को मजबूत बनाने में मदद करता है।
Article 21A was added to the Indian Constitution by the 86th Amendment in 2002. It makes education a fundamental right for children in India. Article 21A says that every child between the ages of 6 and 14 has the right to free and compulsory education. This means it is the responsibility of the government to ensure that every child gets a chance to go to school and does not have to pay for it. It is not just about enrolling children in school, but also about providing good-quality education. To implement this right, the government passed the Right to Education Act, 2009 (RTE Act), which also requires private schools to reserve 25% of seats for children from poor families. The right to education is not just about reading and writing, but also about giving children a respectful and supportive environment to study, and helping them become responsible citizens of society. Article 21A ensures that no child is deprived of education because of poverty or any other reason. In this way, this right protects the future of children and helps in building a strong nation.
अनुच्छेद 22: गिरफ्तारी के समय अधिकार
Article 22: Protection against arrest and detention
अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान का एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने के समय उसके अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद दो तरह की स्थितियों के लिए अधिकार देता है — एक सामान्य गिरफ्तारी और दूसरी ‘प्रतिवंधात्मक निरोध’ (Preventive Detention)। सामान्य गिरफ्तारी के मामले में यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के तुरंत बाद कारण बताए जाने चाहिए और उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। साथ ही, कोई भी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। व्यक्ति को अपने पक्ष में वकील की मदद लेने का अधिकार भी है।
दूसरी ओर, अनुच्छेद 22 ‘प्रतिवंधात्मक निरोध’ यानी ऐसी गिरफ़्तारी को भी अनुमति देता है जो किसी अपराध को होने से रोकने के लिए की जाती है। हालांकि, इसमें भी सीमाएं तय की गई हैं। सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रख सकती है। इसके बाद यदि हिरासत बढ़ानी हो तो विशेष सलाहकार बोर्ड की अनुमति ज़रूरी होती है, और यह अवधि अधिकतम 12 महीने (सामान्य मामलों में) तक हो सकती है। हालांकि संसद चाहे तो कुछ मामलों में इसे 2 साल तक बढ़ा सकती है।
इस प्रकार अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों का उल्लंघन न हो और सरकार भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही गिरफ्तारी या निरोध कर सके। यह अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।
Article 22 is a fundamental right in the Indian Constitution that protects the rights of a person at the time of arrest or detention. This article gives rights in two situations — one is a normal arrest, and the other is ‘preventive detention’. In the case of a normal arrest, Article 22 says that the person must be informed of the reasons for arrest immediately and must be presented before a magistrate within 24 hours. No one can be kept in custody for more than 24 hours without the magistrate’s permission. The person also has the right to consult and be defended by a lawyer of their choice.
On the other hand, Article 22 also allows ‘preventive detention’, which means arresting someone to prevent a possible crime. However, even preventive detention has limits. The government can keep a person in preventive detention without trial for up to 3 months. If it needs to be extended beyond that, the approval of an Advisory Board is required, and it can extend up to a maximum of 12 months (in ordinary cases). In some special cases, Parliament can allow it up to 2 years.
Thus, Article 22 ensures that no one’s liberty or rights are violated without proper legal process, and even the government must follow the law when arresting or detaining a person. This article balances individual freedom and the security of the state in a democracy.
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार | Right Against Exploitation (Articles 23–24)
अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और बेगारी पर प्रतिबंध
Article 23: Prohibition of Human Trafficking and Forced Labour
अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो समाज के सबसे कमजोर और शोषित वर्गों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद मानव तस्करी, ज़बरदस्ती मजदूरी (बेगारी), और किसी भी प्रकार के जबरन श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाता है। मानव तस्करी का मतलब है — किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बेचना-खरीदना, खासकर देह व्यापार या बंधुआ मजदूरी के लिए। बेगारी का मतलब है — बिना उचित भुगतान के किसी से जबरदस्ती काम कराना। भारत में आज़ादी से पहले और बाद में भी कई जगह गरीब और कमजोर लोगों से ज़बरदस्ती मुफ्त में काम कराया जाता था या उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था।
अनुच्छेद 23 यह सुनिश्चित करता है कि ऐसा कोई काम किसी से भी नहीं कराया जा सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा। यह अधिकार न केवल सरकार के खिलाफ लागू होता है बल्कि किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ भी लागू होता है। मतलब, कोई अमीर आदमी, ज़मींदार या कंपनी भी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकती। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति या समूह मानव तस्करी या बेगारी करवाता है तो उसके खिलाफ सज़ा हो सकती है।
सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए कानून बना सकती है और ज़रूरत पड़ने पर खास कानून बनाकर ऐसे अपराधों को रोक सकती है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना और किसी भी तरह के शोषण से बचाना है।
Article 23 is an important fundamental right in the Indian Constitution, created to protect the most vulnerable and exploited sections of society. This article completely prohibits human trafficking, forced labour, and any form of bonded labour. Human trafficking means buying or selling a person forcibly, often for prostitution or bonded work. Forced labour (begar) means making someone work without proper payment or against their will. Before and even after independence, in many parts of India, poor and weak people were forced to work for free or kept as bonded labourers.
Article 23 ensures that no such exploitation can happen to anyone, and if someone does it, it is a punishable offence under the law. This right is enforceable not just against the government but also against private individuals or organizations. This means no rich person, landlord, or company can force anyone to work without consent or proper wages.
The government also has the power to make laws to enforce this article and take special measures to stop such crimes. The main purpose of Article 23 is to give every person the chance to live with dignity and to protect them from any kind of exploitation.
अनुच्छेद 24: बाल श्रम पर रोक
Article 24: Prohibition of Child Labour
अनुच्छेद 24 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो बच्चों को शोषण और खतरनाक कामों से बचाने के लिए बनाया गया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खान या किसी भी ऐसे खतरनाक काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक हो। भारत में लंबे समय तक गरीब बच्चों को पढ़ाई की जगह कम उम्र में ही मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता था, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था।
इस अनुच्छेद का उद्देश्य यही है कि छोटे बच्चों से ऐसा काम न कराया जाए, जिससे उनका बचपन छीने, उनकी पढ़ाई रुके और उनका स्वास्थ्य खराब हो। हालांकि यह अनुच्छेद केवल खतरनाक और जोखिम भरे कामों पर रोक लगाता है। इसलिए सरकार ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और उसके बाद 2016 में संशोधित कानून बनाकर बाल श्रम पर और कड़े प्रतिबंध लगाए। अब कई तरह के घरेलू कामों और दुकानों में बच्चों से मजदूरी कराना भी अपराध माना जाता है।
अनुच्छेद 24 बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार पढ़ाई करे, खेलें और सुरक्षित बचपन जीए। यह अनुच्छेद हमारे समाज के भविष्य यानी बच्चों को सम्मान और सुरक्षा देने का वादा करता है।
4. धर्म की स्वतंत्रता | Right to Freedom of Religion (Articles 25–28)
अनुच्छेद 25: धर्म की स्वतंत्रता
Article 25: Freedom of Religion
अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है, जो हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म को मान सके, उसका पालन कर सके, उसका प्रचार-प्रसार कर सके और अपने धर्म के अनुसार पूजा-पद्धति कर सके। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बदलने या न बदलने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और इस मामले में सरकार या कोई और उसे मजबूर नहीं कर सकता।
अनुच्छेद 25 यह अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से देता है — चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था (public order), शालीनता (morality) और स्वास्थ्य (health) को बनाए रखने के लिए इस अधिकार पर कुछ उचित सीमाएं लगा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का धार्मिक आचरण समाज में अशांति फैलाता है या किसी और के अधिकारों का हनन करता है, तो सरकार उसे रोक सकती है।
इसके अलावा सरकार सामाजिक सुधारों और पिछड़ी प्रथाओं को खत्म करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे — सती प्रथा, बाल विवाह या छुआछूत जैसी प्रथाओं को धर्म के नाम पर कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। अनुच्छेद 25 इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का अधिकार मिले और कोई भेदभाव न हो। इस तरह यह अनुच्छेद हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों का सम्मान करने की परंपरा को बनाए रखता है।
Article 25 is a fundamental right in the Indian Constitution that gives every person the freedom of religion. This article states that every person living in India is free to profess, practice, and propagate any religion of their choice, and to follow their own way of worship. It means that no one can be forced to change their religion, nor can anyone be stopped from following their religion, as long as it does not harm others.
Article 25 gives this right equally to everyone — regardless of which religion they belong to. It guarantees personal religious freedom. However, this freedom is not unlimited. The government can impose reasonable restrictions to maintain public order, morality, and health. This means that if someone’s religious practices disturb peace in society or violate others’ rights, the government can step in to stop it.
The government can also make laws to reform society and stop backward practices. For example, practices like sati, child marriage, or untouchability cannot be justified in the name of religion. Article 25 also ensures equality among all religions and prevents discrimination. In this way, Article 25 protects the secular character of India and respects all religions equally.
अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता
Article 26: Freedom to Manage Religious Affairs
अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि धार्मिक संस्थाओं को भी उनके अधिकार देता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों और संस्थाओं को यह स्वतंत्रता देता है कि वे अपने धर्म से जुड़े मामलों को स्वतंत्र रूप से चला सकें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हर धर्म के लोग न केवल खुद धर्म मानें, बल्कि अपने धार्मिक संस्थानों को भी बिना भेदभाव के प्रबंधित कर सकें।
अनुच्छेद 26 के तहत हर धार्मिक समूह को चार अधिकार दिए गए हैं:
1. अपने धर्म के लिए धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार।
अनुच्छेद 26 का पहला अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि हर धार्मिक समुदाय या संप्रदाय को यह स्वतंत्रता है कि वह अपने धर्म से संबंधित धार्मिक और चैरिटेबल (परोपकार के) उद्देश्यों के लिए संस्थान या संगठन स्थापित कर सके और उन्हें बनाए रख सके।
इसका मतलब यह है कि कोई भी धार्मिक समूह अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मठ, आश्रम, धर्मशाला, गौशाला, अनाथालय, विद्यालय, अस्पताल या कोई भी ऐसी संस्था बना सकता है जिसका उद्देश्य धार्मिक या परोपकारी हो।
सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक कि वह संस्था सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन न करे।
यह अधिकार इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी धार्मिक समूह अपने धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी संस्थाएँ संचालित करे और अपने समुदाय की सेवा कर सके।
2. धार्मिक मामलों का प्रबंधन अपने तरीके से करने का अधिकार।
अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन अपने तरीके से करें।
इसका मतलब यह है कि कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धर्म और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-पद्धतियाँ, आयोजनों और मंदिरों-मठों जैसे धार्मिक संस्थानों का संचालन खुद तय कर सकता है।
कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार यह तय नहीं कर सकती कि वे किस तरीके से पूजा करें, कौन पुजारी हो, किस समय अनुष्ठान हों, कौन नियम बनाए।
हालांकि, इस अधिकार का उपयोग भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए ही किया जा सकता है।
अगर किसी धार्मिक समुदाय की कोई परंपरा समाज में हिंसा फैलाती हो, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हो या कानून का उल्लंघन करती हो, तो सरकार रोक लगा सकती है।
लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, धार्मिक समुदाय अपने धर्म के अनुसार अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं।
3. धार्मिक संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखने और उनका प्रशासन करने का अधिकार।
अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदायों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपनी धार्मिक संपत्तियों को अपने नियंत्रण में रखें और उनका प्रशासन (प्रबंधन) खुद करें।
इसका मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय या समूह के पास जो संपत्तियाँ हैं — जैसे मंदिर की जमीन, मठों की संपत्ति, गुरुद्वारों की जमीन, दान से मिली संपत्तियाँ या बैंक खातों में जमा पैसा — उन पर उनका ही अधिकार रहेगा और वे ही यह तय करेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाए।
सरकार या कोई बाहरी व्यक्ति उनके इस अधिकार में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक धार्मिक समुदाय सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहा हो।
यह अधिकार धार्मिक संस्थाओं को यह स्वतंत्रता देता है कि वे अपनी संपत्तियों का रखरखाव करें, उसका हिसाब रखें और उसका उपयोग अपने धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए करें।
इसका उद्देश्य यह है कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों पर उनका ही नियंत्रण बना रहे और किसी तरह का अनुचित हस्तक्षेप न हो।
4. धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संपत्ति अर्जित करने और उसका उपयोग करने का अधिकार।
अनुच्छेद 26 का चौथा अधिकार धार्मिक समुदायों को यह अधिकार देता है कि वे धार्मिक और परोपकारी (चैरिटेबल) उद्देश्यों के लिए संपत्ति अर्जित करें और उसका उपयोग करें।
इसका मतलब यह है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय या संस्था अपने धार्मिक कामों या समाज सेवा के कामों के लिए संपत्ति (जमीन, भवन, दान, धन आदि) खरीद सकता है, दान के रूप में प्राप्त कर सकता है और उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग भी कर सकता है।
जैसे मंदिरों के लिए ज़मीन ख़रीदना, स्कूल या अस्पताल के लिए बिल्डिंग लेना, अनाथालय चलाने के लिए संसाधन जुटाना — इन सबके लिए संपत्ति रखने और उसका उपयोग करने का अधिकार धार्मिक संस्थाओं के पास है।
सरकार उनकी इस संपत्ति को जबरदस्ती नहीं ले सकती, न ही उनके उपयोग में अनुचित हस्तक्षेप कर सकती है।
हालांकि, यह अधिकार भी अन्य सभी अधिकारों की तरह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन ही है।
इसका उद्देश्य यह है कि धार्मिक संस्थाएँ स्वतंत्र होकर अपने धर्म और समाज सेवा के कामों के लिए संसाधन जुटा सकें और उनका सही उपयोग कर सकें।
हालांकि, इस अनुच्छेद के अधिकार भी पूरी तरह असीमित नहीं हैं। इनका उपयोग भी सार्वजनिक व्यवस्था (public order), नैतिकता (morality) और स्वास्थ्य (health) के नियमों के अधीन रहकर ही किया जा सकता है। अगर किसी धार्मिक संस्था की गतिविधियाँ समाज में हिंसा फैलाती हैं, कानून तोड़ती हैं या असामाजिक होती हैं, तो सरकार इन्हें रोक सकती है।
अनुच्छेद 26 यह सुनिश्चित करता है कि सभी धर्मों की संस्थाएँ अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करें और सरकार उनके आंतरिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। यह हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखता है और सभी धर्मों को समान सम्मान देने का संदेश देता है।
Article 26 is an important fundamental right in the Indian Constitution, which protects not just individuals but also religious institutions and gives them the freedom to manage their own affairs. Since India is a secular country, the Constitution ensures that people of every religion can not only practice their faith but also manage their religious institutions without discrimination.
Article 26 gives four main rights to every religious group:
1. To establish and maintain religious and charitable institutions.
The first right under Article 26 ensures that every religious denomination or group has the freedom to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes.
This means any religious community can set up and run its own temples, mosques, churches, gurudwaras, monasteries, ashrams, dharamshalas, cow shelters, orphanages, schools, hospitals, or any other institution meant for religious or charitable purposes.
The government cannot interfere in this right as long as the activities of the institution do not violate public order, morality, or health.
This right guarantees that every religious group can freely carry out its religious practices and serve its community through its own institutions.
2. To manage their own religious affairs in their own way.
Under Article 26, religious communities also have the right to manage their own religious affairs in their own way.
This means any religious group can conduct its rituals, ceremonies, festivals, and manage its temples, monasteries, or other religious institutions according to its faith and customs.
No outsider or even the government can dictate how they should perform their worship, who should be the priest, what rules to follow, or how their ceremonies should be conducted.
However, this right too is subject to public order, morality, and health.
If any practice of the community causes violence, harms public health, or violates the law, the government can step in.
But as long as these conditions are met, religious communities are free to manage their religious affairs as per their beliefs.
3. To own and administer property belonging to the religious institution.
Under Article 26, religious communities are also given the right to own and administer their properties and manage them on their own.
This means that any property belonging to a religious denomination — such as land of a temple, property of a monastery, land and buildings of a gurudwara, donations, or money in bank accounts — remains under their control, and they have the right to decide how it will be used.
The government or any outsider cannot interfere with this right as long as the religious group follows public order, morality, and health.
This right gives religious institutions the freedom to maintain their property, keep accounts, and use it for religious or charitable purposes.
The purpose of this right is to ensure that the property of religious institutions remains under their own management without undue interference.
4. To acquire property and use it for religious and charitable purposes.
The fourth right under Article 26 allows religious communities to acquire property and use it for religious and charitable purposes.
This means any religious denomination or institution can buy property (like land, buildings), receive donations, or collect funds for its religious activities or for social service activities like running schools, hospitals, orphanages, etc.
They also have the right to use such property as per their own objectives.
The government cannot forcibly take away their property or interfere unduly in its use.
However, just like the other rights, this right is also subject to public order, morality, and health.
The purpose of this right is to allow religious institutions to freely gather resources and use them for promoting religion as well as for the welfare of society.
However, these rights are also subject to public order, morality, and health. This means if the activities of a religious institution disturb peace, break laws, or harm society, the government can intervene.
Article 26 ensures that all religious institutions can function independently according to their faith, and the government does not interfere in their internal religious matters. This article protects the secular character of India and promotes equal respect for all religions.
अनुच्छेद 27: धार्मिक करों पर रोक
Article 27: Freedom from Paying Religious Taxes
अनुच्छेद 27 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति सरकार को किसी धर्म विशेष के प्रचार या पालन के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा टैक्स या कर नहीं वसूल सकती, जिसका उपयोग किसी धर्म के कामों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी धार्मिक आयोजन को चलाने के लिए किया जाए।
यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष (secular) देश है और सरकार का काम सभी धर्मों के बीच समानता बनाए रखना है, न कि किसी एक धर्म का प्रचार करना। इसलिए अगर सरकार को कोई टैक्स वसूलना है तो उसका उपयोग केवल सार्वजनिक सेवाओं के लिए होना चाहिए — जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा आदि। सरकार इस टैक्स का उपयोग किसी धार्मिक संस्था के निर्माण, रखरखाव या किसी धार्मिक आयोजन के खर्च के लिए नहीं कर सकती।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार धार्मिक संस्थाओं के लिए सुविधाएं या सुरक्षा बिल्कुल नहीं दे सकती। सरकार जरूरत पड़ने पर सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को सामान्य सुविधाएं या सुरक्षा दे सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति से विशेष धर्म के लिए टैक्स लेना संविधान के खिलाफ है।
इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि लोगों को अपने पैसे से सिर्फ उस धर्म का प्रचार करने के लिए मजबूर न किया जाए, जिसे वे नहीं मानते। यह धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के सम्मान की गारंटी देता है।
Article 27 is an important fundamental right in the Indian Constitution. It ensures that no person in India can be forced to pay taxes to promote or maintain any particular religion. This means the government cannot collect any tax from citizens if that money is going to be used for religious purposes like maintaining temples, mosques, churches, gurudwaras, or conducting religious events.
This article makes sure that India remains a secular country and the government treats all religions equally. Any tax collected by the government must only be used for public purposes — like roads, schools, hospitals, security, etc. It cannot be used to fund the promotion or maintenance of any religion.
However, this does not mean the government cannot provide basic facilities or security to religious places. It only means no person can be forced to pay taxes specifically for the promotion of a religion they do not follow.
The aim of this article is to protect people from being compelled to support any particular religion through taxes, and to uphold the secular nature of the country while respecting all religions equally.
अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता और प्रतिबंध
Article 28: Freedom in Religious Education
अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो यह तय करता है कि सरकारी और सरकार द्वारा वित्त पोषित (funded) शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति को बनाए रखना और सभी धर्मों का समान सम्मान सुनिश्चित करना है।
अनुच्छेद 28 के अनुसार शिक्षण संस्थानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
1. पूरी तरह से सरकारी धन से चलने वाले शिक्षण संस्थान:
ऐसे संस्थानों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उदाहरण: सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज।
2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेकिन पूरी तरह सरकारी नहीं (सरकार द्वारा आंशिक सहायता प्राप्त) संस्थान:
ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसी भी छात्र को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा लेने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
3. पूरी तरह से निजी और अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान:
ऐसे संस्थानों में उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वे अपने धर्म के अनुसार शिक्षा दें।
इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि किसी भी छात्र पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी धर्म विशेष की शिक्षा थोपना न हो। खासकर सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी धर्मों के छात्रों के साथ समानता हो और किसी एक धर्म का पक्ष न लिया जाए।
Article 28 is an important provision of the Indian Constitution, which deals with how religious education can or cannot be imparted in educational institutions run or funded by the government. The aim is to maintain India’s secular character and ensure equal respect for all religions.
According to Article 28, educational institutions are divided into three categories:
1. Institutions fully funded by the government:
Religious instruction is completely prohibited in these institutions. Example: government schools and colleges.
2. Institutions recognized by the government but not fully funded (partially aided):
Religious instruction may be given here, but no student can be forced to take part in religious education or religious ceremonies against their will.
3. Fully private and minority-run institutions:
These institutions have full freedom to provide religious education according to their faith.
The purpose of this article is to ensure that no student is compelled to follow or learn any particular religion against their choice. By prohibiting religious education in fully government-run institutions, it ensures equality among students of all religions and prevents the government from favoring any one religion.
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार | Cultural & Educational Rights (Articles 29–30)
अनुच्छेद 29: संस्कृति की रक्षा का अधिकार
Article 29: Protection of Culture
अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जो भारत की विविधता और सभी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है। हमारा देश कई भाषाओं, लिपियों, परंपराओं और संस्कृतियों से भरा हुआ है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसका प्रचार-प्रसार करने के अधिकार से वंचित न हो।
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में रहने वाले किसी भी हिस्से के नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
इसका मतलब यह है कि चाहे कोई अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, कोई भी समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोने के डर के बिना अपने रीति-रिवाज, भाषा और परंपराओं को आगे बढ़ा सकता है।
इसके अलावा अनुच्छेद 29 यह भी कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल भाषा, धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर किसी शैक्षिक संस्थान में दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
इस तरह यह अनुच्छेद भारत की एकता में विविधता को बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर समुदाय अपने अस्तित्व और पहचान को बचाए रख सके।
Article 29 is an important right in the Indian Constitution that protects the cultural identity of all communities in India. Our country is full of different languages, scripts, traditions, and cultures. The purpose of this article is to make sure that no person or group is denied the right to preserve and promote their language, script, and culture.
This article states that any section of citizens living in any part of India has the right to conserve their own language, script, and culture.
This means that whether a community is a minority or majority, it can continue its customs, language, and traditions without fear of losing its cultural identity.
In addition, Article 29 also provides that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained or aided by the state just because of their language, religion, caste, or culture.
Thus, this article preserves India’s unity in diversity and ensures that every community can protect and sustain its unique identity.
अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार
Article 30: Right of Minorities to Establish Educational Institutions
अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है, जो भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार देता है।
भारत में अनेक धर्म और भाषाओं वाले लोग रहते हैं। इनमें से कई छोटे-छोटे समूह (अल्पसंख्यक) हैं, जिनकी भाषा, परंपरा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अधिकार दिया गया।
अनुच्छेद 30 कहता है कि —
धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार है कि वे अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करें और उनका प्रशासन (प्रबंधन) करें।
इसका मतलब यह है कि चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों (जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी) या भाषाई अल्पसंख्यक (जैसे जिनकी भाषा बहुसंख्यक भाषा से अलग है), उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार है।
इसके अलावा, अगर सरकार उनकी जमीन या संपत्ति अधिग्रहित करती है या उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करती है तो उन्हें मुआवजा देना अनिवार्य है।
यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिलाता है कि उनकी शिक्षा और संस्कृति की रक्षा संविधान के तहत होगी।
इसका उद्देश्य यही है कि देश के सभी लोग, चाहे वे कितने भी छोटे समुदाय से हों, अपनी पहचान को बनाए रखें और अपनी अगली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और शिक्षा दे सकें।
Article 30 is a special provision in the Indian Constitution that gives minority communities in India the right to establish and administer educational institutions of their choice.
India has many religions and languages, and several small groups (minorities) whose language, tradition, and education need protection and promotion.
Article 30 states that —
All minorities, whether based on religion or language, have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
This means that religious minorities (like Muslims, Christians, Sikhs, Parsis) and linguistic minorities (whose language is different from the majority) can set up and run schools, colleges, and other educational institutions according to their culture and traditions.
Moreover, if the government takes their property or interferes with their rights, it must provide them proper compensation.
This article assures minorities that their education and cultural identity will be protected under the Constitution.
The main purpose of this article is to ensure that even small communities can preserve their unique identity and pass on their culture and education to future generations.
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार
Right to Constitutional Remedies (Article 32)
अनुच्छेद 32: मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार
Article 32: Right to Constitutional Remedies
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक बेहद महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे “मौलिक अधिकारों का रक्षक” भी कहा जाता है।
इस अनुच्छेद के तहत अगर किसी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार (Fundamental Right) किसी सरकारी संस्था या किसी अन्य के द्वारा छीना जाता है, तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकता है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का “मूल आत्मा (heart & soul)” कहा था, क्योंकि यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार केवल कागज़ पर न रह जाएं, बल्कि उनका पालन भी हो।
अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति अदालत से इन न्यायिक आदेशों (writs) के लिए आवेदन कर सकता है:
- हबीयस कॉर्पस (Habeas Corpus) — किसी को गैरकानूनी तरीके से कैद से छुड़वाना।
- मैंडेमस (Mandamus) — सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कहना।
- प्रोहिबिशन (Prohibition) — निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना।
- क्वो वारंटो (Quo Warranto) — किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किसी सरकारी पद पर किस अधिकार से बैठा है।
- सरटिओरारी (Certiorari) — निचली अदालत से रिकॉर्ड मंगाकर उसका परीक्षण करना और गलत आदेश रद्द करना।
यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ चुप न रहे और अदालत की मदद ले सके।
हालांकि, राष्ट्रीय आपातकाल (Emergency) की स्थिति में सरकार अनुच्छेद 32 के अधिकार को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकती है।
इसका उद्देश्य यह है कि हर नागरिक को यह भरोसा हो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतें हमेशा उपलब्ध हैं।
Article 32 is one of the most important rights in the Indian Constitution, and is also called the “protector of fundamental rights.”
Under this article, if a person’s fundamental rights are violated by any government authority or anyone else, they can directly approach the Supreme Court or the High Court to seek justice.
Dr. B.R. Ambedkar called Article 32 the “heart and soul” of the Constitution, because it ensures that the fundamental rights given to citizens are not just written on paper but are actually enforced.
Under Article 32, a person can request the court to issue the following writs:
- Habeas Corpus — to release a person from illegal detention.
- Mandamus — to direct a government officer to perform their duty.
- Prohibition — to stop a lower court from acting beyond its authority.
- Quo Warranto — to question the authority of a person holding a public office.
- Certiorari — to review and nullify wrong decisions of lower courts.
This article ensures that no citizen has to remain silent against the violation of their rights and can always seek help from the courts.
However, during a national emergency, the government can temporarily suspend the right to move courts under Article 32.
The purpose of this article is to assure every citizen that the courts are always there to protect their constitutional rights.
डॉ. अम्बेडकर ने इसे “संविधान की आत्मा (Soul of the Constitution)” कहा था।
अंतिम अनुच्छेद:
अनुच्छेद 33–35: संसद द्वारा अधिकार सीमित करने की शक्ति
Articles 33–35: Power of Parliament to modify fundamental rights in specific cases
संसद कुछ खास परिस्थितियों में (जैसे: सेना, पुलिस) के लिए मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है।
Parliament can restrict fundamental rights in the case of armed forces, police, etc., for discipline and security.
संक्षेप में:
| Fundamental Right | Hindi | English |
|---|---|---|
| Article 14–18 | समानता | Equality |
| Article 19–22 | स्वतंत्रता | Freedom |
| Article 23–24 | शोषण से मुक्ति | Against Exploitation |
| Article 25–28 | धर्म की स्वतंत्रता | Freedom of Religion |
| Article 29–30 | सांस्कृतिक अधिकार | Cultural Rights |
| Article 32 | संवैधानिक उपचार | Constitutional Remedies |
अनुच्छेद 33: सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों की सीमा
Article 33: Limitation of Fundamental Rights for Armed Forces
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और इसी प्रकार के अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को आवश्यक सीमा तक सीमित कर सके। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि इन बलों में अनुशासन, कार्यकुशलता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखी जा सके, क्योंकि यदि इन बलों के सदस्यों को सामान्य नागरिकों की तरह सभी मौलिक अधिकार दिए जाएं, जैसे हड़ताल करने, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने या सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, तो इससे इन बलों की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी कारण संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून बनाकर यह तय कर सके कि किन अधिकारों को, कितनी सीमा तक इन बलों के सदस्यों के लिए सीमित करना उचित होगा। इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि सशस्त्र बल और अन्य सुरक्षा बल पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें।
Article 33 of the Indian Constitution empowers Parliament to enact laws to the extent necessary to restrict the fundamental rights of members of the armed forces, paramilitary forces, police, intelligence agencies, and similar services. This provision ensures that discipline, efficiency, and national security are maintained, as granting these forces unrestricted rights like ordinary citizens — such as the right to strike, participate in political activities, or organize public protests — could negatively impact their effectiveness and endanger national security. Therefore, Parliament is authorized to determine, by law, the extent to which such rights should reasonably be curtailed for members of these forces. Laws enacted under this article ensure that armed and security forces perform their duties with full dedication and discipline, safeguarding the sovereignty and integrity of the nation.
एक सैनिक को सरकार की आलोचना करने की आज़ादी नहीं होती, भले ही वाणी की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है।
A soldier cannot criticize the government publicly, even though freedom of speech is a fundamental right.
अनुच्छेद 34: मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों की सीमा
Article 34: Restriction of Rights during Martial Law
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर यह तय कर सके कि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किस हद तक रोक लगाई जाएगी और उन अधिकारों का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। मार्शल लॉ तब लागू किया जाता है जब देश के किसी हिस्से में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो जाए और सामान्य प्रशासन हालात को संभालने में असमर्थ हो। ऐसी स्थिति में सेना को पूरे प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए जाते हैं ताकि वह स्थिति को नियंत्रित कर सके और शांति व्यवस्था बहाल कर सके। इस दौरान सेना को अनुशासन और प्रभावशीलता के लिए विशेष अधिकार दिए जाते हैं, और जरूरी होने पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे आंदोलन, भाषण, सभा आदि पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सेना और उसके अधिकारियों द्वारा मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों के लिए उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करे, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निडर होकर कर सकें। इसके अलावा संसद यह भी तय कर सकती है कि नागरिकों को मुआवज़ा देने की कोई व्यवस्था होगी या नहीं।
Article 34 of the Indian Constitution empowers Parliament to make laws specifying the extent to which fundamental rights of citizens may be restricted and how they will be exercised in an area where martial law is in force. Martial law is imposed when the civil administration fails completely, and the military is entrusted with full administrative control to restore order and maintain peace. During this period, the military is granted special powers, and fundamental rights such as freedom of movement, speech, or assembly may be temporarily curtailed if required for maintaining discipline and control. Article 34 authorizes Parliament to provide legal protection to the actions of the military and its personnel during martial law so that they can discharge their duties fearlessly. It also allows Parliament to decide whether or not to provide compensation to citizens affected by such actions. This ensures that the military can effectively maintain national security and order during extreme situations while keeping the authority with the Parliament to regulate such measures.
ऐसे समय में, अगर सेना कानून के अनुसार कोई कार्य करती है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा।
During such time, actions taken lawfully by military cannot be challenged in court.
अनुच्छेद 35: संसद को विशेष अधिकार
Article 35: Power of Parliament to make laws related to Fundamental Rights
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को विशेष अधिकार देता है कि वह कुछ विशेष मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर कानून बनाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन अधिकारों के संबंध में पूरे देश में एक समान कानून लागू हो और अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न कानून बनकर संविधान के उद्देश्य को प्रभावित न करें। अनुच्छेद 35 यह स्पष्ट करता है कि संविधान में जहाँ-जहाँ यह कहा गया है कि किसी अधिकार के प्रयोग के लिए या उस पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए संसद कानून बनाएगी, वहाँ वह शक्ति केवल संसद के पास होगी और राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद यह तय कर सकती है कि किन परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में निवास (residence) के आधार पर विशेष प्रावधान किए जाएं। इसी तरह अनुच्छेद 32 में संसद यह तय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 33 और 34 के तहत भी संसद को ही यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों और मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर क्या सीमाएँ लगाई जाएँ, यह तय करे। इसके अलावा संसद को ही यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 23 (मानव तस्करी पर रोक) और अनुच्छेद 24 (बाल श्रम पर रोक) को लागू करने के लिए दंडात्मक कानून बनाए।
Article 35 of the Indian Constitution grants Parliament the exclusive power to make laws on certain matters related to fundamental rights. The purpose of this provision is to ensure uniformity of laws across the country in these specific areas, avoiding different states enacting conflicting laws. Article 35 clarifies that wherever the Constitution specifies that Parliament shall make a law to regulate or restrict the exercise of a particular fundamental right, that power vests solely in Parliament and not in state legislatures. For example, under Article 16(3), Parliament can determine the conditions for making residence-based provisions in public employment. Similarly, under Article 32, Parliament can prescribe the procedure for enforcing writs by the Supreme Court. Parliament alone is also empowered under Articles 33 and 34 to decide the extent of restrictions on fundamental rights of armed forces and during martial law. Additionally, Parliament has the exclusive power to enact penal laws to implement Articles 23 (prohibition of human trafficking) and 24 (prohibition of child labour). This ensures that the fundamental rights framework remains uniform and effective throughout India.
सारांश | Summary:
| अनुच्छेद | विषय (Hindi) | Topic (English) |
|---|---|---|
| 33 | सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करना | Limit rights of Armed Forces |
| 34 | मार्शल लॉ के दौरान अधिकार सीमित करना | Restrict rights during Martial Law |
| 35 | सिर्फ संसद को अधिकार | Parliament has exclusive power for FR laws |
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव बताना न भूलें। हमारे साथ जुड़कर और भी महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करें!
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समझना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। उम्मीद है यह लेख आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें। धन्यवाद! 🙏